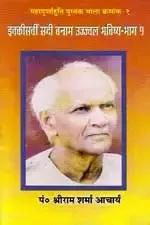|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> इक्कीसवीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 1 इक्कीसवीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 1श्रीराम शर्मा आचार्य
|
420 पाठक हैं |
||||||
गुरुदेव की अमृतवाणी....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भूमिका
पिछले दिनों बड़े विज्ञान और बुद्धिवाद ने मनुष्य के लिए अनेक असाधारण
सुविधाएँ प्रदान की है, किन्तु सुविधाएँ बढ़ाने के उत्साह में हुए इनके
अमर्यादित उपयोगों की प्रतिक्रियाओं ने ऐसे संकट खड़े कर दिए हैं, जिनका
समाधान न निकला, तो सर्वविनाश प्रत्यक्ष जैसा दिखाई पड़ता है।
इस सृष्टि का कोई नियंता भी है। उसने अपनी समग्र कलाकारिता बटोर कर इस धरती को और उसकी व्यवस्था के लिए मनुष्य को बनाया है। वह इसका विनाश होते देख नहीं सकता। नियंता ने सामयिक निर्णय लिया है कि विनाश को निरस्त करके संतुलन की पुनः स्थापना की जाए।
सन् 1989 से 2000 तक युग संधिकाल माना गया है। सभी भविष्यवक्ता, दिव्यदर्शी इसे स्वीकार करते हैं। इस अवधि में हर विचारशील, भावनाशील, प्रतिभावान को ऐसी भूमिका निभाने के लिए तैयार-तत्पर होना है। जिससे वे असाधारण श्रेय सौभाग्य के अधिकारी बन सकें।
इस सृष्टि का कोई नियंता भी है। उसने अपनी समग्र कलाकारिता बटोर कर इस धरती को और उसकी व्यवस्था के लिए मनुष्य को बनाया है। वह इसका विनाश होते देख नहीं सकता। नियंता ने सामयिक निर्णय लिया है कि विनाश को निरस्त करके संतुलन की पुनः स्थापना की जाए।
सन् 1989 से 2000 तक युग संधिकाल माना गया है। सभी भविष्यवक्ता, दिव्यदर्शी इसे स्वीकार करते हैं। इस अवधि में हर विचारशील, भावनाशील, प्रतिभावान को ऐसी भूमिका निभाने के लिए तैयार-तत्पर होना है। जिससे वे असाधारण श्रेय सौभाग्य के अधिकारी बन सकें।
किंकर्त्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियाँ
विज्ञान और बुद्धिवाद बीसवीं सदी की बड़ी उपलब्धियाँ हैं। उनसे
सुविधा-साधनों के नए द्वार भी खुले, वस्तुस्थिति समझने में, सहायक स्तर की
बुद्धि का विकास भी हुआ, पर साथ ही दुरुपयोग का क्रम चल पड़ने से इन दोनों
ही युग चमत्कारों ने लाभ के साथन पर नई हानियाँ, समस्याएँ और विपत्तियाँ
उत्पन्न करनी आरंभ कर दीं। उत्पादनों को खपाने के लिए आर्थिक उपनिवेशवाद
का सिलसिला चल पड़ा। युद्ध उकसाए गए, ताकि उनमें अतिरिक्त उत्पादनों को
झोंका-खपाया जा सके। कुशल कारीगरी ने स्थान तो पाया, गृह उद्योगों के
सहारे जीवनयापन करने वाली जनता की रोटी छिन गई। काम के अभाव में आज बड़ी
संख्या में लोग बेकार-बेरोजगार हैं। परिस्थितियाँ गरीबी की रेखा से
दिनोंदिन नीचे गिरती जा रही हैं, यो बढ़ तो अमीरों का अमीरी भी रही है।
कारखाने और द्रुतगामी वाहन निरन्तर विषैला धुआँ उगल कर वायुमंडल को जहर से भर रहे हैं। उनमें जलने वाले खनिज ईंधन का इतनी तेजी से दोहन हुआ है कि समूचा खनिज भंडार एक शताब्दी तक भी और काम देता नहीं दीख पड़ता। धातु और रसायनों के उत्खनन से भी पृथ्वी उन संपदाओं से रिक्त हो रही है। उन्हें गँवाने के साथ-साथ धरातल की महत्वपूर्ण क्षमता घट रही है और उसका प्रभाव धरती के उत्पादन से गुजारा करने वाले प्राणियों पर पड़ रहा है। जलाशयों में बढ़ते शहरों का, कारखानों का कचरा, उसे अपेय बना रहा है। साँस लेते एवं पानी पीते यह आशंका सामने खड़ी रहती है कि उसके साथ कहीं मंद विषों की भरमार शरीरों में न हो रही हो ? उद्योगों-वाहनों द्वारा छोड़ा गया प्रदूषण ‘‘ग्रीन हाउस इफेक्ट’’ के कारण अंतरिक्ष में अतिरिक्त तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे हिम प्रदेशों की बर्फ पिघल जाने और समुद्रों में बाढ़ आ जाने का खतरा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मांडीय किरणों की बौछार से पृथ्वी की रक्षा करने वाला ओजोन कवच, विषाक्तता का दबाव न सह सकने के कारण, फटता जा रहा है, क्रम वही रहा, तो जिन सूर्य किरणों से पृथ्वी पर जीवन का विकास क्रम हुआ है, वे ही छलनी के अभाव में अत्यधिक मात्रा में आ धमकने का कारण विनाश भी उत्पन्न कर सकती हैं।
अणु-ऊर्जा विकसित करने का जो नया उपक्रम चल पड़ा है, उसने विकिरण फैलाना तो आरंभ किया ही है, यह समस्या भी उत्पन्न कर दी है कि उनके द्वारा उत्पन्न राख को कहाँ पटका जाएगा ? जहाँ भी वह रखी जाएगी, वहाँ संकट खड़े करेगी।
कारखाने और द्रुतगामी वाहन निरन्तर विषैला धुआँ उगल कर वायुमंडल को जहर से भर रहे हैं। उनमें जलने वाले खनिज ईंधन का इतनी तेजी से दोहन हुआ है कि समूचा खनिज भंडार एक शताब्दी तक भी और काम देता नहीं दीख पड़ता। धातु और रसायनों के उत्खनन से भी पृथ्वी उन संपदाओं से रिक्त हो रही है। उन्हें गँवाने के साथ-साथ धरातल की महत्वपूर्ण क्षमता घट रही है और उसका प्रभाव धरती के उत्पादन से गुजारा करने वाले प्राणियों पर पड़ रहा है। जलाशयों में बढ़ते शहरों का, कारखानों का कचरा, उसे अपेय बना रहा है। साँस लेते एवं पानी पीते यह आशंका सामने खड़ी रहती है कि उसके साथ कहीं मंद विषों की भरमार शरीरों में न हो रही हो ? उद्योगों-वाहनों द्वारा छोड़ा गया प्रदूषण ‘‘ग्रीन हाउस इफेक्ट’’ के कारण अंतरिक्ष में अतिरिक्त तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे हिम प्रदेशों की बर्फ पिघल जाने और समुद्रों में बाढ़ आ जाने का खतरा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मांडीय किरणों की बौछार से पृथ्वी की रक्षा करने वाला ओजोन कवच, विषाक्तता का दबाव न सह सकने के कारण, फटता जा रहा है, क्रम वही रहा, तो जिन सूर्य किरणों से पृथ्वी पर जीवन का विकास क्रम हुआ है, वे ही छलनी के अभाव में अत्यधिक मात्रा में आ धमकने का कारण विनाश भी उत्पन्न कर सकती हैं।
अणु-ऊर्जा विकसित करने का जो नया उपक्रम चल पड़ा है, उसने विकिरण फैलाना तो आरंभ किया ही है, यह समस्या भी उत्पन्न कर दी है कि उनके द्वारा उत्पन्न राख को कहाँ पटका जाएगा ? जहाँ भी वह रखी जाएगी, वहाँ संकट खड़े करेगी।
स्थिति निश्चित ही विस्फोटक
यह विज्ञान को उत्कर्ष के साथ ही उसके दुरुपयोग की कहानी है, जिसमें सुखद
अंश कम और दुःखद भाग अधिक है। वह उपक्रम अभी भी रुका नहीं है, वरन्
दिन-दिन उसका विस्तार ही हो रहा है। अब तक जो हानियाँ सामने आईं हैं, जो
समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं का समाधान हाथ नहीं लग रहा है, फिर इस
सबका अधिकाधिक संवर्धन अगले ही दिनों न जाने क्या दुर्गति उत्पन्न करेगा ?
इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय के वैज्ञानिक दुरुपयोग
का क्या नतीजा निकला और अगले दिनों उसकी अभिवृद्धि से और भी क्या अनर्थ हो
सकने की आशंका है ?
विज्ञान का दर्शन प्रत्यक्षवाद पर अवलम्बित है। उसने दर्शन को भी प्रभावित किया है और मान्यता विकसित की है कि जो कुछ सामने है, उसी को सब कुछ माना जाए। इसका निष्कर्ष आज के प्रत्यक्ष लाभ को प्रधानता देता है। परोक्ष का अंकुश अस्वीकार कर देने पर ईश्वर, धर्म और उसके साथ जुड़े हुये संयम, सदाचार और पुण्य-परमार्थ के लिए कोई भी स्थान नहीं रह जाता। मर्यादाओं और वर्जनाओं को अंधविश्वास कह कर, उनसे पीछा छुड़ाने पर इसलिए जोर दिया गया है कि इससे व्यक्ति की निजी सुविधाओं में कमी आती है। पूर्ति का सिद्धान्त यही कहता है कि जिस प्रकार भी, जितना भी लाभ उठाया जा सके, उठाना चाहिए, जिसमें सिद्धान्त को आड़े नहीं आने देना चाहिए। इसी मान्यता ने पशु-पक्षियों के वध को स्वाभाविक प्रक्रिया बनाकर असंख्यों गुना बढ़ा दिया गया है। अन्य प्राणियों के प्रति निष्ठुरता बरतने के उपरान्त जो बाँध टूटता है, वह मनुष्यों के साथ निष्ठुरता न बरतने का कोई सैद्धान्तिक कारण शेष नहीं रहने देता। मनुष्य को पशु-प्रवृत्तियों का वहनकर्त्ता ठहरा देने के उपरान्त यौन स्वेच्छाचार न बरतने के पक्ष में भी कोई ठोस दलील नहीं रह जाती।
विज्ञान और बुद्धिवाद की नई धाराएँ खोजने के लिए और उनके आधार पर तात्कालिक लाभ के जादू-चमत्कार प्रस्तुत करने वाली आधुनिकता, नीति और सदाचार का एक सिरे से दूसरे सिरे तक उन्मूलन करती, मनुष्य को स्वेच्छाचार बनाती जा रही है।
विज्ञान का दर्शन प्रत्यक्षवाद पर अवलम्बित है। उसने दर्शन को भी प्रभावित किया है और मान्यता विकसित की है कि जो कुछ सामने है, उसी को सब कुछ माना जाए। इसका निष्कर्ष आज के प्रत्यक्ष लाभ को प्रधानता देता है। परोक्ष का अंकुश अस्वीकार कर देने पर ईश्वर, धर्म और उसके साथ जुड़े हुये संयम, सदाचार और पुण्य-परमार्थ के लिए कोई भी स्थान नहीं रह जाता। मर्यादाओं और वर्जनाओं को अंधविश्वास कह कर, उनसे पीछा छुड़ाने पर इसलिए जोर दिया गया है कि इससे व्यक्ति की निजी सुविधाओं में कमी आती है। पूर्ति का सिद्धान्त यही कहता है कि जिस प्रकार भी, जितना भी लाभ उठाया जा सके, उठाना चाहिए, जिसमें सिद्धान्त को आड़े नहीं आने देना चाहिए। इसी मान्यता ने पशु-पक्षियों के वध को स्वाभाविक प्रक्रिया बनाकर असंख्यों गुना बढ़ा दिया गया है। अन्य प्राणियों के प्रति निष्ठुरता बरतने के उपरान्त जो बाँध टूटता है, वह मनुष्यों के साथ निष्ठुरता न बरतने का कोई सैद्धान्तिक कारण शेष नहीं रहने देता। मनुष्य को पशु-प्रवृत्तियों का वहनकर्त्ता ठहरा देने के उपरान्त यौन स्वेच्छाचार न बरतने के पक्ष में भी कोई ठोस दलील नहीं रह जाती।
विज्ञान और बुद्धिवाद की नई धाराएँ खोजने के लिए और उनके आधार पर तात्कालिक लाभ के जादू-चमत्कार प्रस्तुत करने वाली आधुनिकता, नीति और सदाचार का एक सिरे से दूसरे सिरे तक उन्मूलन करती, मनुष्य को स्वेच्छाचार बनाती जा रही है।
बढ़ती आबादी, बढ़ते संकट
यह सब बातें कामुकता को प्राकृतिक मनोरंज मानने और उसे उन्मुक्त रूप से
अपनाने के पक्ष में की जाती है। फलतः बंधनमुक्त यौनाचार जनसंख्या में
वृद्धि की नई विभीषिका खड़ी कर रहा है। गर्भ निरोध से लेकर भ्रूण हत्याओं
तक को प्रोत्साहन मिलने के बाद भी जनसंख्या चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से
बढ़ रही है। एक के चार, चार के सोलह, सोलह से चौसठ बनते-बनते संख्या न
जाने कहाँ तक पहुँचेगी। तीन हजार वर्ष पहले मात्र तीस करोड़ व्यक्ति सारे
संसार में थे, अब तो वह छः सौ करोड़ हो गए हैं। लगता है कि अगले बीस
वर्षों में कम से कम दूने होकर ऐसा संकट उत्पन्न करेंगे, जिसमें मकान का,
आहार का संकट तो रहेगी ही, रस्तों पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा।
पृथ्वी पर सीमित संख्या में ही प्राणियों को निर्वाह देने की क्षमता है। वह असीम प्राणियों को पोषण नहीं दे सकती। बढ़ता हुआ जन समुदाय अभी भी ऐसे अगणित संकट खड़े कर रहा है। खाद्य उत्पादन के लिए भूमि कम पड़ती जा रही है। आवास के लिए बहुमंजिले मकान बन रहे हैं, फिर भी खेती के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी भूमि की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ रही है। जंगल बुरी तरह कट रहे हैं। उसमें घिरी हुई जमीन को खाली करने की आवश्यकता, कानूनी रोकथाम के होते हुए भी किसी न किसी तरह पूरी हो रही है।
वन कटते जा रहे है। फलस्वरूप वायुप्रदूषण की रोकथाम का रास्ता बंद हो रहा है। जमीन में जड़ों की पकड़ न रहने से हर साल बाढ़े आती हैं, भूमि कटती है, रेगिस्तान बनते हैं। नदियों की गहराई कम होते जाने से पानी का संकट सामने आता है। फर्नीचर, मकान और जलावन तक के लिए लकड़ी मुश्किल हो रही है। वन काटने की अनेक हानियों को जानते हुए भी, आवास के लिए खाद्य के लिए सड़कों, स्कूलों और बाँधों के लिए जमीन तो चाहिए ही। यह सब जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम ही तो हैं। इन्हीं में से एक अनर्थ और भी जुड़ जाता है, शहरों की आबादी का बढ़ना। बढ़ते हुए शहर, घिसपिच की गंदगी के कारण नरक तुल्य बनते जा रहे हैं।
पृथ्वी पर सीमित संख्या में ही प्राणियों को निर्वाह देने की क्षमता है। वह असीम प्राणियों को पोषण नहीं दे सकती। बढ़ता हुआ जन समुदाय अभी भी ऐसे अगणित संकट खड़े कर रहा है। खाद्य उत्पादन के लिए भूमि कम पड़ती जा रही है। आवास के लिए बहुमंजिले मकान बन रहे हैं, फिर भी खेती के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी भूमि की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ रही है। जंगल बुरी तरह कट रहे हैं। उसमें घिरी हुई जमीन को खाली करने की आवश्यकता, कानूनी रोकथाम के होते हुए भी किसी न किसी तरह पूरी हो रही है।
वन कटते जा रहे है। फलस्वरूप वायुप्रदूषण की रोकथाम का रास्ता बंद हो रहा है। जमीन में जड़ों की पकड़ न रहने से हर साल बाढ़े आती हैं, भूमि कटती है, रेगिस्तान बनते हैं। नदियों की गहराई कम होते जाने से पानी का संकट सामने आता है। फर्नीचर, मकान और जलावन तक के लिए लकड़ी मुश्किल हो रही है। वन काटने की अनेक हानियों को जानते हुए भी, आवास के लिए खाद्य के लिए सड़कों, स्कूलों और बाँधों के लिए जमीन तो चाहिए ही। यह सब जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम ही तो हैं। इन्हीं में से एक अनर्थ और भी जुड़ जाता है, शहरों की आबादी का बढ़ना। बढ़ते हुए शहर, घिसपिच की गंदगी के कारण नरक तुल्य बनते जा रहे हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book